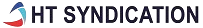नयी दिल्ली , फरवरी 02 -- विज्ञान और साहित्य के जरिये पारिस्थितिकी वैज्ञानिक मध्यकालीन भारतीय कविताओं की मदद से पारिस्थितिकी के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।
साइंस डेली में रविवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखी गयी कविताएं और लोकगीत पश्चिमी भारत के लंबे घास के मैदान को समझने में मदद कर रहे हैं। ये घास के मैदान भारत के लगभग 10 प्रतिशत क्षेत्र में फैले हुए हैं। दशकों तक कई वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं का यह मानना था कि ये क्षेत्र कभी जंगल थे, जो मानवीय गतिविधियों से नष्ट हो गये। इसी धारणा ने बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में वृक्षारोपण की रणनीतियों को आकार दिया।
नये शोध से एक अलग कहानी सामने आती है। ऐतिहासिक साहित्य संकेत देते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बर्बाद हुए जंगल नहीं हैं, बल्कि अपने आप में लंबे समय से चले आ रहे पारिस्थितिकी तंत्र हैं। सार्वजनिक धारणा और आधिकारिक नीति दोनों में, भारत और अन्य स्थानों पर ऐसे क्षेत्रों को अक्सर 'बंजर भूमि' के रूप में 'चिन्हित' किया गया है। उन्हें आमतौर पर क्षतिग्रस्त जंगलों के रूप में देखा जाता है।
ऐतिहासिक साक्ष्य एक अलग कहानी बताते हैं। शोधकर्ताओं ने प्राचीन ग्रंथों में 44 जंगली पौधों की प्रजातियों के संदर्भों की पहचान की, जिनमें से लगभग दो-तिहाई इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के विशिष्ट पौधे हैं।
इसका एक उदाहरण लगभग 16वीं शताब्दी के महाकाव्य 'आदि पर्व' में मिलता है। पाठ में निरा नदी घाटी की समृद्ध घास के कारण वहां आकर्षित होने वाले चरवाहों का वर्णन है, जिसे 'खाली' और 'कांटेदार' बताया गया है। एक अन्य वृत्तांत पंढारपुर के तीर्थ स्थल पर 15वीं शताब्दी के एक कवि-संत की समाधि से उगने वाले 'तरटी' वृक्ष का वर्णन करता है, जिसे वैज्ञानिक 'कैपरिस डिवैरीकाटा' के नाम से जानते हैं।
कवि चक्रधर द्वारा उल्लिखित बबूल के पेड़ का भी बार-बार उल्लेख मिलता है। टीम को इस कांटेदार प्रजाति के आठ संदर्भ मिले, जिसे 'वाचेलिया ल्यूकोफ्लोया' के नाम से जाना जाता है, जिसमें पंख जैसे पत्ते, हल्के पीले रंग की छाल और सफेद फूल होते हैं।
कुल मिलाकर, ये ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि भारत के लंबे घास के मैदान कम से कम 750 वर्षों से अस्तित्व में हैं। वे ब्रिटिश शासन के दौरान बड़े पैमाने पर हुई वनों की कटाई से बहुत पहले ही स्थापित हो चुके थे।अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य और भी गहरे इतिहास की ओर इशारा करते हैं। जीवाश्म और दरियाई घोड़े जैसे घास खाने वाले जानवरों के अवशेष संकेत देते हैं कि हजारों साल पहले इस क्षेत्र में घने जंगलों के बजाय इस प्रकार की लंबी घास का वर्चस्व था।
ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी की पत्रिका 'पीपल एंड नेचर' में प्रकाशित एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पश्चिमी भारत की ऐतिहासिक कथाओं में पौधों के दिये गये संदर्भों का परीक्षण किया। उनका लक्ष्य यह समझना था कि अतीत में वहां किस प्रकार की वनस्पतियां मौजूद थीं।
मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्ययन लेखक आशीष नेर्लेकर ने कहा, "मेरे लिए मुख्य बात यह है कि चीजें कितनी कम बदली हैं। यह दिलचस्प है कि सैकड़ों साल पुरानी कोई चीज़ आज के परिवेश से इतनी करीब से मेल खा सकती है।"पुणे के भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) में पुरातत्व के पीएचडी छात्र दिग्विजय पाटिल ने पवित्र स्थलों से संबंधित संस्कृत और मराठी ग्रंथों का अध्ययन करते समय कुछ असामान्य पौधों को बार-बार पाया। पादप वैज्ञानिक श्री नेर्लेकर ने उनमें से कई पौधों को उन प्रजातियों के रूप में पहचाना जो आज भी लंबी घास के मैदान में सामान्य रूप से पाई जाती हैं।
शोध दल ने मराठी में लिखे या गाए गए लोक गीतों, कविताओं और मिथकों की समीक्षा शुरू की, जिनमें से कुछ 13वीं शताब्दी के हैं। इनमें से अधिकांश सामग्री आधुनिक डेटाबेस में संग्रहीत नहीं है, जो पारिस्थितिक जानकारी का एक अनछुआ स्रोत है।
इनमें से कई कृतियाँ महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, जहाँ लगभग 37,485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अब खुले घास के मैदान हैं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित